OUR PRODUCTS
Our Products

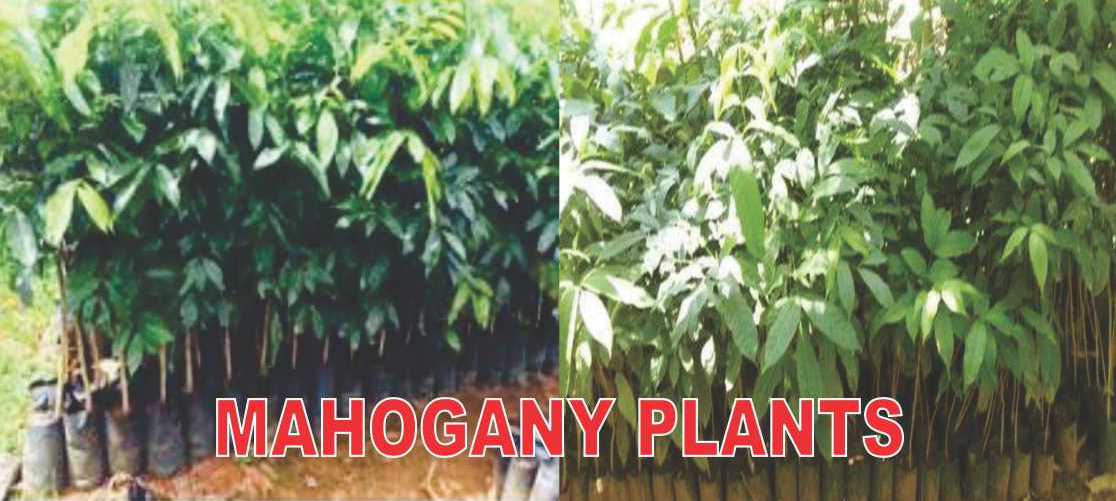
भारतीय कृषि विकास पथ में है। 75% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र से बाहर आए हैं किसानों ने अनेक तरह की फसलों को लगाकर उत्पादन तथा आय में कमी रहने के कारण कृषि कार्य छोड़ दिया है, इसके साथ-साथ प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियाँ भी एक कारण बन गई हैं, परंतु आज कल के शिक्षित तथा जागरूक किसानों ने उत्पादन तथा आय में लगातार समान रूप से लाभ देने वाले उत्तम गुणवत्ता युक्त लकड़ी के पौधे लगा रहे हैं। इस पौधों की देखरेख करना भी बाकी वाणिज्य फसलों से आसान है। वितरण तथा मांग के बीच में अंतर बढ़ने के कारण गुणवत्ता युक्त लकड़ी की मांग दिन-ब-दिन बढ़ रही है। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन परिस्थितियों के अनुकूल ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले आनुवंशिक रूप से गुणवत्ता युक्त मोहगनी के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं।
आनुवंशिक रूप से गुणवत्ता युक्त मोहगनी-
जीनस स्वतेनियां की उष्णकटबंधीय द्वण लकड़ी प्रजातियों की एक सीधे बनिहार लाल भूरे रंग की इमारती लकड़ी है जो अमेरिका का स्थानीय वृक्ष है। चिनबेरी फैमिली मेलियासी परिवार का हिस्सा है।
आनुवंशिक उत्तम श्रेणी पौधों के लक्षण-
1. उत्तम श्रेणी के पौध गुणवत्ता युक्त रंगीन लकड़ी को कम समय में देते हैं।
2. अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण यह समान रूप से विकास करते हैं।
3. मुख्य तना 50 से 70 फीट लंबा और 4 से 4.5 फ़ीट मोटा होता है।
ग्रीन भूमि की विशेषताएं-
20 इकाइयों से ज्यादा खरीदने वाले किसानों को ग्रीन भूमि मुफ्त में आवश्यक तकनीकी समाचार देती है। यह सुविधा प्रथम 1 वर्ष तक ही सीमित है।
विपणन पद्धति-
दलाल को निकालने के लिए ग्रीन भूमि के पहचान-पत्र युक्त वितरक आपको वितरण करता है।
मोहगनी-
यह एक इमारती लकड़ी है। इस लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर, जहाज, मूर्तियां एवं सजावट की चीजों को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग शक्तिवर्धक दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। यह पेड़ 40 से 60 फीट की लम्बाई तक जाता है। यह पेड़ ऊसर और जलभराव भूमि को छोड़कर सभी जमीन पर लगाया जाता है। इस लकड़ी पर पानी का कोई असर नहीं होता। यह पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता रखता है। इस वृक्ष को ज्यादा बारिश की भी जरूरत नहीं होती। इस पेड़ को 5 से 7 फीट की दूरी पर रोपाई की जाती है। इस वृक्ष की कटाई 12 साल बाद की जाती है। इस वृक्ष की कटाई जड़ के पास से ही की जाती है। यह पेड़ 30 से 35 क्यूबिक फिट लकड़ी देता है। मुख्य तना 50 से 60 फीट लंबाई, 35 से 45 इंच गोलाई होती है। 1 एकड़ में 800 पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी लकड़ी ₹ 2000 से ₹ 2500 प्रति घट फ़ीट में जाती है। इस प्रकार 1 एकड़ से एक से सवा करोड़ की आमदनी की जा सकती है।
विशेषताएं-
1. महोगनी पौधे लगाने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
2. इन आनुवंशिक उत्तम गुणवत्ता युक्त पौधों के वास्तविक विकास उत्पादन तथा आय भूमि की उपजाऊ तथा प्रबंधन पद्धतियों पर आधारित है।
3. जल ग्रस्त छारीय मिट्टी इस पौधे के लिए अनुकूल नहीं है।
4. पौधे लगाने से पहले किसान को मिट्टी परीक्षण करके पौधा लगाना चाहिए।
एक यूनिट = 10 पौधे
बिक्री रेट ₹ 1090 प्रति यूनिट
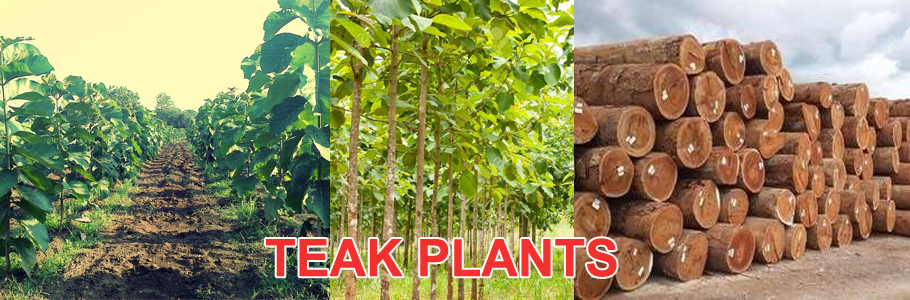
सागौन के पौधे :-
सागौन या टीकवुड द्विबीजपत्री पौधा है। यह चिरहरित यानी वर्ष भर हरा रहने वाला पौधा है। सागौन का वृक्ष प्राय: 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसका वृक्ष काष्ठीय होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफी समय तक चलने वाली होती है। इसके पत्ते काफी बड़े होते हैं। फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस यह बहुमूल्य इमारती लकड़ी है।
संस्कृत में इसे शाक कहते हैं लगभग 2 सहस्त्र वर्षों से भारत में यह ज्ञात है और अधिकता से व्यवहृत होती जा रही है वर्बीनैसी कुल का यह वृहत पर्णपाती वृक्ष है। यह शाखा और शिखर पर ताज ऐसा चारों तरफ फैला हुआ होता है। भारत वर्मा और थाईलैंड का देशज है। पर फिलीपाइन द्वीप, जावा और मलाया प्रायद्वीप में भी पाया जाता है भारत में आरावली पहाड़ में पश्चिम में पूर्वी देशांतर अर्थात झांसी तक में पाया जाता है। आसाम और पंजाब में यह सफलता से उगाया गया है। साल में 50 इंच से अधिक वर्षा वाले और 25 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान वाले स्थानों में यह अच्छा उपजता है। जिसके लिए 3000 फुट की ऊंचाई के जंगल अधिक उपयुक्त है। सब प्रकार की मिट्टी में यह उपज सकता है पर पानी का निकास रहना अथवा अधोभूमि का सूखा रहना आवश्यक है। गर्मी में इसकी पत्तियां झड़ जाती है गर्म स्थानों में जनवरी में ही पत्तियां गिरने लगती हैं पर अधिकांश स्थानों में मार्च तक पत्तियां हरी भरी रहती हैं पत्तियां 1 से 2 फीट लंबी और 6 से 12 इंच चौड़ी होती है इसका लच्छेदार फूल सफेद या कुछ नीलापन लिए सफेद होता है। बीज गोलाकार होते हैं और पक जाने पर गिर पड़ते हैं। बीज में तेल रहता है बीज बहुत धीरे-धीरे अंकुरित होते हैं साधारणतया 100 से 150 फुट ऊंचे और धड़ 3 से 8 फुट ब्यास के होते हैं।
धड़ की छाल आधा इंच मोटी, धूसर या भूरे रंग की होती है। इनका रसकाष्ठ सफेद एवं अंतरूकाष्ठ हरे रंग का होता है। अंतरूकाष्ठ की गंध सुहावनी और प्रबल सौरभ वाली होती है। गंद बहुत दिनों तक कायम रहती है।
सागौन की लकड़ी बहुत अल्प सिकुड़ती और बहुत मजबूत होती है इस पर पॉलिश जल्द चढ़ जाती है जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है कई 100 वर्ष पुरानी इमारतों में यह ज्यों की त्यों पाई जाती है दो सहस्त्र वर्षों के पश्चात भी सागौन की लकड़ी अच्छी अवस्था में पाई गई है। सागौन के अंतकाष्ठ को दीमक आक्रांत नहीं करती यद्दपि रसकाष्ठ को खा जाती है।
सागौन उत्कृष्ट कोटि के जहाजों, नावो, बोगियों इत्यादि भवनों की खिड़कियों और चौखट, रेल के डिब्बों और उत्कृष्ट कोटि के फर्नीचर के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
अच्छी भूमि पर 2 वर्ष पुराने पौध जो 5 से 10 फीट ऊंचे होते हैं लगाए जाते हैं और लगभग 60 वर्षों में यह औसत 60 फुट का हो जाता है और इसके धड़ का व्यास डेढ़ से 2 फुट का हो सकता है। बर्मा में 80 वर्ष की उम्र के पेड़ का घेरा 2 फीट व्यास का हो जाता है यद्यपि भारत में इतना मोटा होने के लिए 200 वर्ष लग सकते हैं। भारत में ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास, कुर्ग, मैसूर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जंगलों के सागौन की उत्कृष्ट लकड़ियां अधिकांश बाहर चली जाती हैं। वर्मा का सागौन पहले पर्याप्त मात्रा में भारत आता था पर अब वहां से भी बाहर चला जाता है।

पपीता रेड लेडी, उत्पादन विधि :-
भूमि और जलवायु:
पपीता के उत्पादन के लिए अच्छी जलनिकास उच्चआद्रता वाली भूमि अच्छी मानी जाती है। पपीता के उत्पादन के लिए भूमि का पी.एच. 5.5 से 7 उपयुक्त माना जाता है। जिस भूमि में जल धारण क्षमता की कमी हो वहां पपीते की फसल अच्छी नहीं होती। ऐसी भूमि में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और उत्पादन घट जाता है। पपीता के अच्छे उत्पादन के लिए आद्रता की अधिकता एवं कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा वाली भूमि अच्छी मानी जाती है। चूना पत्थर युक्त जमीन में पपीता के पौधे बढ़ नहीं पाते, ऐसी भूमि में क्षारीय पदार्थ कम होते हैं। पपीता की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म एवं आद्रता वाली जलवायु होनी चाहिए। सामान्यतः 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता 60% हो तो ऐसे में पपीता की अच्छी पैदावार होती है और उत्पादन भारी मात्रा में मिलता है। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बुवाई उपयुक्त होती है।
निम्नलिखित गुणधर्म पाए जाने वाले पौधे लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं :
सामान्यतः 40 से 80 दिन के पौधे। 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। 6 से 15 पत्तियों वाले पौधे।
रोपड़:
1. पौध अंतरण लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और दो पौधों के बीच की दूरी 2 मीटर रखते हैं।
2. पौध लगाने के लिए गड्ढे बनाना : गड्ढे 1'1'1 आकार के बनाए जाएं इन गड्ढे में 100 ग्राम मिट्टी में मिला कर गड्ढे में भर देना चाहिए।
इस तरह बनाए गए हर गड्ढे में केवल एक पौध प्लास्टिक बैग थैला से निकालकर लगाएं। रोपाई करते समय जड़ सहित पौधा गड्ढे में लगाए, पौधे लगाने के लिए एक दिन पहले पौधों को पानी दे और रोपाई के बाद पौधे में पूरी सिंचाई करनी चाहिए। पौधों की रोपाई सुबह या शाम को हल्की धूप में ही करें।
सिंचाई:
पपीता पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है पानी की कमी के कारण फूल और फल गिरने लगते हैं पपीता के पौधे में सिंचाई मिट्टी की किस्म और तापमान पर निर्भर करती है भूमि प्रकार और जलवायु को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। सामान्यतया गर्मी में 5 से 7 दिन में एक बार और सर्दी में 10 से 15 दिन में 1 बार पानी दिया जाए।
खाद एवं उर्वरक प्रयोग:
निम्नलिखित खाद की मात्रा प्रति पौधा इस प्रकार की जाए :
1. पौधे लगाने के हर 2 माह बाद 2 टोकरी गोबर की खाद रिंग विधि से दी जाए।
2. माह में एक बार कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान मैगनीज, लौह और जिंक युक्त उर्वरक फौवारा द्वारा छिड़काव करें।
फल की तुड़ाई:
पौधे लगाने के बाद 8 से 10 माह में रेड लेडी पपीता का फल तोड़ने योग्य हो जाता है। ऐसे फलों का रंग गहरा हरा से हल्का हरा होकर हल्के पीले रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर की डंठल सहित फल तोड़ लें। ध्यान रहे कि ज्यादातर पलों को सुबह 9 से सायं 3 के बीच में निकाला जाए। फलों को मंडी में भेजने के लिए उन्हें अच्छी तरह पेपर में लपेट लें।
आय-व्यय
18 से 20 महीने तक एक पेड़ 100 से 160 किलो तक फल देता है। लाभ किसान की प्रबंधन क्षमता जलवायु मिट्टी, दवाओं आदि पर निर्भर करता है यदि 1000 पौधा औसत 100 किलो फल देता है तो कुल उत्पादन 100000 किलो प्राप्त होगा तथा बाजार मूल्य ₹5 प्रति किलो से गुणा किया जाए तो कुल लाभ ₹500000 प्राप्त होने की संभावना रहती है। 1 एकड़ का अधिकतम खर्च ₹55,000 यदि घटाया जाए तो शुद्ध आए ₹445,000 प्रति एकड़ संभव है।
नर व मादा:
वर्णिता किस्म में नर पौधे नहीं हैं। सभी फल देने वाले पौधे होते हैं तथा इसमें परंपरागण हेतु नर पौधों की आवश्यकता नहीं होती। अपवादस्वरूप अफलनशील पौधे नगण्य हो जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना:
जहां वर्षा की अधिकता और मिट्टी में पानी लगने की समस्या हो वहां पर पपीता की रोपाई नहीं करनी चाहिए। जलजमाव वाली मिट्टी पपीता के लिए हानिकारक है।
नोट-
यहां दी गई जानकारियां और लक्ष्य हमारे परीक्षण एवं प्रयोग पर आधारित हैं भिन्न स्थानों पर भिन्न मौसम, भूमि प्रकार एवं ऋतू के कारण परिणाम बदल सकते हैं।
विशेषताएं:
जल्द बढ़ने वाला एवं अधिक उपज देने वाला पौधा।
फल का आकार - गोल एवं लंबा कार।
फल का रंग - आकर्षक हरा एवं फल पकने पर लाल रंग का दिखाई देता है।
फल का गूदा - आकर्षक लाल और मीठा स्वाद।
फल का औसत वजन - लगभग 1.5 से 2.5 किग्रा।
इस फल की छाल (ऊपरी परत) - मोटी होने के कारण लंबी यातायात के लिए उपयुक्त है।
पल तुड़ाई की अवधि - पौधा लगाने के 8 से 10 महीने उपरांत फल परिपक्व हो जाता है।
पौधरोपण - 2 मीटर x 2 मीटर।
पौधे की संख्या - प्रति एकड़ 1200 पौधे।

आम:-
आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आम उगाने वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है किंतु सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आकर्षक रंग, स्वाद और सुगंध वाला यह फल ए व बी का प्रचुर स्रोत है। भारत में पके आम की खपत लगभग 12 किग्रा प्रति व्यक्ति है। इसका प्रयोग फल की हर अवस्था में किया जाता है, कच्चा आम चटनी, अचार व अनेक प्रकार के पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अनेक प्रकार के जैम, जेली, सीरप और नेक्टर बनाए जाते हैं।
भूमि एवं जलवायु :
आम हर प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। अच्छे जल निकाल वाली दोमट मिट्टी अच्छी है इनकी अच्छी वृद्धि हेतु 2 से 2.5 मीटर गहरी मृदा की आवश्यकता होती है। आम उष्ण व समशीतोष्ण जलवायु में पैदा होता है तथा समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किया जा सकता है। जहां 4.4 से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है परंतु 23.8 से 26.6 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आदर्श तापमान माना जाता है।
किस्में :
1. मुंबई हरा- यह अगैती किस्म है। इसे मालदा या सरोली भी कहते हैं। फल मध्यम आकार का अंडाकार तथा पकने पर हरापन लिए होता है इसकी भंडारण क्षमता कम होती है।
2. रटौल - यह भी अगैती किस्म है। इसका फल छोटे आकार का अंडाकार रंग हरा पीला सुगंध युक्त मीठा होता है।
3. दशहरी - यह मध्य मौसम की सबसे लोकप्रिय किस्म है। फल मध्यम आकार का रंग हरा पीला मीठा व सुगंध युक्त होता है इसकी भंडारण क्षमता अधिक लगभग 10 दिन है।
4. लंगड़ा - यह भी एक मध्य मौसम की किस्म है। इससे रूहअफजा, दरभंगा तथा हर दिल अजीज भी कहते हैं। फल बड़ा तथा पकने पर हरापन लिए होता है गूदा सुगंध युक्त मीठा होता है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 4 दिन होती है।
5. चौसा - यह पिछेती किस्म है। इसे का कारिया व ख़ाजरी भी कहते हैं। पका फल बड़े आकार का हरा पीला रंग लिए होता है तथा गूदा मीठा व सुगंध-युक्त होता है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 5 दिन है।
6. फजरी - यह भी पिछेती किस्म है। इसे फजली भी कहते हैं। फल का आकार मध्यम तथा रंग पीला होता है गूदा सुगंध-युक्त होता है। इसकी भंडारण क्षमता कम होती है।
7. राम केला - यह देर से पकने वाली किस्म है इसका फल पके पर भी खट्टा होता है। यह चार के लिए सर्वोत्तम किस्म है।
8. मल्लिका - यह किस्म नीलम तथा दशहरी किस्मों के संयोग से विकसित की गई है। यह नियमित रूप से चलने वाली मध्य मौसम की किस्म है इसका फल लंबा बड़ा कैडमियम के रंग की भांति पीला व स्वादिष्ट होता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक है किंतु फलत कम है। इसके फल निर्यात के लिए अच्छे प्रमाणित हो रहे हैं।
9. आम्रपाली - यह दशहरी एवं नीलम किस्मों के संयोग से विकसित की गई है। मध्य मौसम की बौनी व नियमित फसल वाली किस में है। इसके एक हेक्टर में 2.5 x 2.5 मीटर पर 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं।
10. गौरव - यह दशहरी एवं तोता परी किस्मों का शंकर है यह भी मध्य मौसम की किस्म है। फल अत्यंत सुंदर मध्यम आकार का लंबा और पकने पर लाल आभा लिए हुए सुनहरा पीला मीठा व सुगंध युक्त होता है। इसकी फलत कम है किंतु भंडारण क्षमता अधिक होने के कारण इसके सुंदर व स्वादिष्ट फलों को निर्यात किया जाता है।
11. सौरभ - यह दशहरी एवं फजरी जाफरानी के संयोग से विकसित की ही गई है। यह भी मध्य मौसम की किस्म है। फल मध्यम लंबा व पकने पर हरापन लिए यह सुनहरा पीला होता है। गूदा ठोस, रेशा रहित, सुनहरा पीला वा सुगंध युक्त होता है।
12. राजीव - यह दशहरी एवं रूमानी का शंकर है यह जुलाई के तीसरे सप्ताह में पकता है। यह मध्यम रोमानी किस्म के फल जैसा गोल व पकने पर हरा पीला होता है। गूदा मुलायम, नींबू जैसा पीला, रेशा-रहित, खट्टा-मीठा व सुगंध युक्त होता है। अधिक नियमित फलत तथा अपेक्षाकृत हल्का पीला व खटास-युक्त मीठा गूदा होने के कारण फलों को आम उद्योग में प्रयोग किया जा सकता है।
रोपड़
किस्म के अनुसार 07 से 10 मीटर की दूरी पर एक घन मीटर आकार के गड्ढे खोदने चाहिए। इन गड्ढों को तेज धूप में लगभग 5 दिन खुला छोड़ देना चाहिए जिससे उसकी मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया व कीड़े आदि तेज गर्मी से समाप्त हो जाए। तत्पश्चात खाद एवं मिट्टी की समान की समान मात्रा मिश्रण से भरकर सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे गड्ढों की मिट्टी बैठ जाए।

आंवला:-
भूमि - बलुई भूमि के अतिरिक्त सभी प्रकार की भूमियों में आंवला की खेती की जा सकती है। सामान्य भूमि से लेकर उसरीली भूमि जिसका पी.एच. मान 9 तक हो, उसमें आंवला की खेती की जा सकती है।
गड्ढों की खुदाई एवं भराई - ऊसर भूमि में 5-8 मीटर की दूरी पर एक से 1x1x1 फुट आकार के गड्ढे खोद लेने चाहिए। यदि कड़ी परत अथवा कंकड़ की तह हो तो उसे खोदकर अलग कर लेना चाहिए अन्यथा बाद में पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर देना चाहिए है प्रत्येक गड्ढे में 50 से 60 किग्रा गोबर की खाद 15 से 20 किग्रा बालू, 8-10 किग्रा जिप्सम तथा 6 किग्रा पायराइट मिलाना चाहिए। भराई के 5 से 7 दिन बाद अभिक्रिया समाप्त होने पर ही पौधों का रोपण किया जाना चाहिए। वह सामान्य भूमि में प्रत्येक गड्ढे में 2 -3 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, 100 ग्राम नत्रजन, फास्फोरस देना आवश्यक होता है। गड्ढे जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना चाहिए।
आंवला की व्यवसायिक जातियां- आंवला की व्यवसायिक जातियों में चकैया, फ्रांसिस, कृष्णा, कंचन, नरेंद्र आमला-4 , और नरेंद्र आमला-7 एवं गंगा बनारसी उल्लेखनीय है। व्यवसायिक जातियां चकैया एवं फ्रांसिस से काफी लाभार्जन होता है।
खाद एवं उर्वरक- आंवला की फसल बागवानी के लिए प्रतिवर्ष 100 ग्राम नत्रजन, 60 ग्राम फॉस्फोरस , 75 ग्राम पोटाश प्रति वर्ष पेड़ की दर से देते रहना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की यह मात्रा 10 वर्ष तक बढ़ाते रहना चाहिए। उसर भूमि में जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं अतः 2 से 3 वर्ष उर्वरकों के साथ साथ 250 से 500 ग्राम जिंक सल्फेट फलत वाले पौधों में देना चाहिए।
सिंचाई- आंवला के नव रोपित बागों में गर्मी के मौसम में 10 दिन के अंतराल पर पेड़ों की सिंचाई करते रहना चाहिए और फलत वाले बागों में जून माह में एक बार पानी देना चाहिए। फूल आते समय बागों में किसी तरह से पानी नहीं दिया जाना चाहिए। समय-समय पर खरपतवार निकालने हेतु थालों की गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक है।
आंवला से अधिक उपज और आकर्षक फल लेने के उपाय- 1. बागों की उचित देख रहे करें।
2. सामुचित पोषण दें।
3. सितंबर माह में 0.5 प्रतिशत एग्रोमीन एवं 0.5 प्रतिशत पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करें।
4. फलों के मौसम में 1 माह के अंतराल पर डाइथेन M45-0.3 प्रतिशत तथा मैटासिस्टाक्स 0.03 प्रतिशत के छिड़काव अच्छे होते हैं।
5. बोरान तत्व की कमी के लिए 50 ग्राम बोरेक्स प्रति वृक्ष देना आवश्यक है।
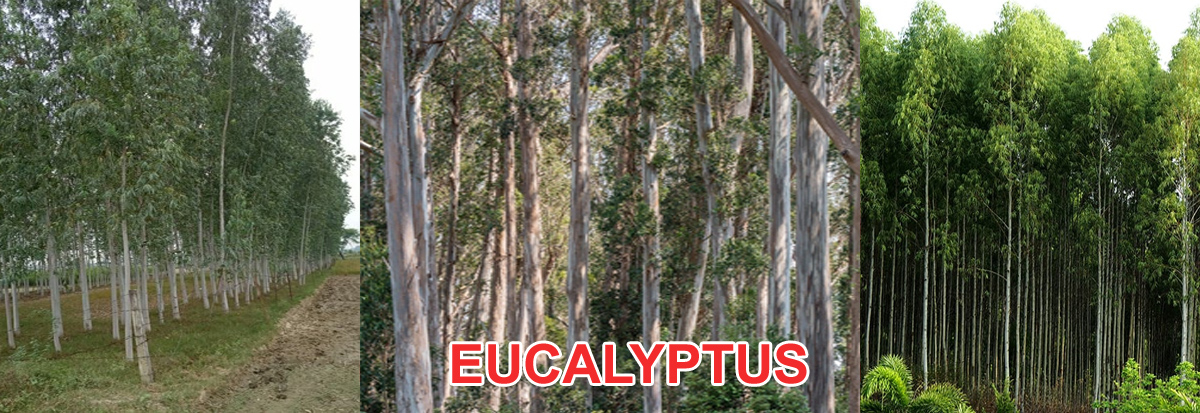
यूकेलिप्टस:-
यूकेलिप्टस - यूकेलिप्टस प्रजाति प्राकृतिक रूप से आस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह तेजी से बढ़ने वाली सीधे छत्र वाली प्रजाति है। इसका प्रयोग इमारती लकड़ी, फर्नीचर, पेटियां, लुगदी, ईधन, पार्टिकल बोर्ड, हार्ड बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है।
मृदा व जलवायु - यूकेलिप्टस जीरो डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 20 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में उग सकता है।
गहरी परत वाली नम मिट्टी व 6.5 से 7.5 पी.एच. मान तक की मिट्टी यूकेलिप्टस लगाने के लिए उत्तम होती है।
हल्के जलभराव वाले क्षेत्रों में भी यूकेलिप्टस उगाया जा सकता है।
नोट - अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधे का प्रयोग में लाना चाहिए। अन्य संस्थानों के अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता के पौधे हमारी कंपनी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
खेतों में पौधरोपण:-
खेतों की मेढों पर - यूकेलिप्टस के पौधे खेतों की मेढों पर 2 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। खेतों की मेधो पर पौधारोपण की दिशा पूर्व पश्चिम हो ताकि सर्दियों में रबी की फसल पर लगातार छाया ना पड़े।
खेत के मध्य में - बंजर अथवा कम उपजाऊ वाली भूमि पर यूकेलिप्टस का सघन वृक्षारोपण 2 मीटर से 2 मीटर के अंतर पर किया जाता है कतारों के मध्य 2 वर्ष तक खेती की जा सकती है कम उपजाऊ भूमि पर भी अच्छा लाभ मिलता है।
आप अपने खेतों की मेड़ों व खेतों में अधिक से अधिक यूकेलिप्टस लगाकर लाभ पाएं।
1. गेहूं व धान गन्ना आदि फसलों के साथ यूकेलिप्टस लगाने पर आपको अतिरिक्त उपज प्राप्त हो सकती है।
2. सामान्यत: 5 वर्ष बाद यूकेलिप्टस के वृक्षों को बेचने से लगभग 2000 से 2500 प्रति वृक्ष की आय होती है।
3. यूकेलिप्टस के तेल, शहद आदि जैसी वन उपज भी प्राप्त होती है।
5 वर्ष पुराना यूकेलिप्टस एक वृक्ष 4 कुंतल इंधन देता है जो आपके परिवार के लिए दो माह तक के लिए खाना बनाने के काम आता है। इस प्रकार आपके खेत में 12 यूकेलिप्टस के पेड़ आपको वर्ष भर का ईंधन देते हैं जिससे पशुओं का गोबर खाद बनाने के काम आता है तथा ईंधन खोजने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। निजी भूमि यूकेलिप्टस वृक्ष उत्तर प्रदेश वन निगम निर्धारित समर्थन मूल्य पर क्रय करता है। उत्तर प्रदेश वन निगम ने यूकेलिप्टस का गोलाई वार मूल्य निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश में अपने खेत में उगाए गए यूकेलिप्टस के वृक्ष काटने व बेचने के लिए वन विभाग अथवा किसी अन्य विभाग से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इटावा, गाजीपुर, मुरादाबाद, सहित प्रदेश के 42 जिलों में यूकेलिप्टस की लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी प्रकार की परमिट अथवा किसी प्रकार का शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है यूकेलिप्टस पौधे को खेत में बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है वृक्ष का छत्र छाया हल्का होने के कारण इसकी छाया बहुत कम होती है पेड़ को काट देने पर पुनः नए कल्ले निकल आते हैं जिससे 5 वर्ष में नया पेड़ तैयार हो जाता है। पेड़ों को जानवर नहीं खाते इससे इनकी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यूकेलिप्टस का पेड़ खेत में लगाकर आप पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में प्रदेश व देश के विकास एवं समृद्धि में योगदान देते हैं।
यूकेलिप्टस के पेड़ पर रहने वाले पक्षी खेती के शत्रु कीट पतंगो, चूहा को नष्ट कर फसल की रक्षा करते हैं खेत की मेड़ों पर लगाए गए यूकेलिप्टस के पौधों को अलग से सिंचाई व खाद देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि खेतों को दिया गया पानी व खाद यूकेलिप्टस को अपने आप ही मिल जाता है।

नींबू:-
1. सीडलेस - फल का साइज बड़ा एवं रस की मात्रा अधिक पाई जाती है।
2. कागजी - इसके ऊपरी परत हल्की तथा फल मध्यम साइज का होता है इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है।
3. विक्रम नींबू कम समय में ज्यादा उत्पादन का साइज होता है।
4. यह दूसरे साल में उत्पादन शुरू हो जाता है 4-5 साल से 100 किग्रा - 125 किग्रा तक फल देता है। आमदनी प्रति पेड़ 2000 से 3000 तक सालाना।

अमरूद:-
1. एल-49 खाने में स्वादिष्ट एवं मीठा होता है और फल का मध्यम आकार होता है।
2. इलाहाबादी फल की पैदावार अधिक होती है एवं भंडारण क्षमता ज्यादा होती है।
3. रायपुरी फल का साइज बड़ा आता है और बीज की मात्रा कम होती है दूसरे साल से फलना आरंभ हो जाता है।

विमल 149 अनार:-
1. कम समय में फल उत्पादन करना शुरू कर देता है।
2. यह रूबी कल्टीवर की अच्छी किस्म से तैयार किया गया है।
3. इसका फल लाल कत्थई रंग तथा चमकता रहता है।
4. 170 ग्राम तक के बड़े फल आते हैं।
5. यह अधिक स्वादिष्ट और मीठा होता है।
6. रस की मात्रा अधिक पाई जाती है।
7. यह दूसरे साल से फल देना शुरू कर देता है।

स्वर्ण चीकू:-
1. तीसरे साल से उत्पादन आरंभ तथा अधिक उत्पादन देता है।
2. बड़े एवं अंडाकार वाला फल होता है।
3. नारंगी रंग का गूदा बेहतर स्वाद।
4. रोग प्रतिरोधक क्षमता और विपरीत प्रभाव से लड़ने की क्षमता रखता है।
5. कम जगह में ज्यादा पौधे लगाकर अधिक लाभ।
© Green Bhoomi Plantation 2026, All right reserved. Website Powered by Deal4U Team






